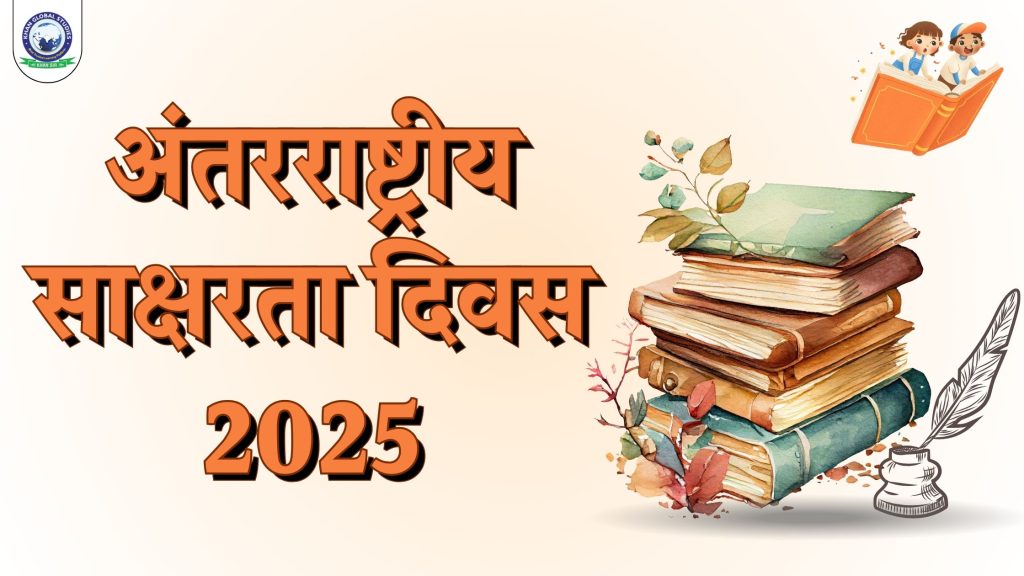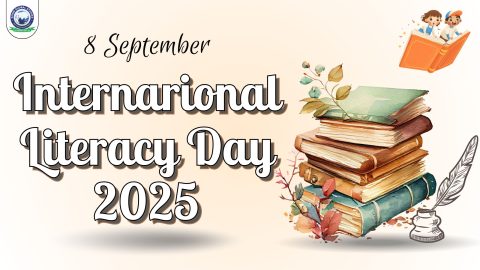हर साल 8 सितंबर को विश्वभर में अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। यह दिन साक्षरता की महत्ता को उजागर करता है और हमें याद दिलाता है कि पढ़ना-लिखना मात्र एक कौशल नहीं, बल्कि हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है।
साक्षरता किसी भी व्यक्ति के जीवन में स्वावलंबन, समाज में भागीदारी और समृद्धि का आधार होती है। आज के डिजिटल युग में, जहां हर कार्य डिजिटल माध्यम से संचालित होता है, साक्षरता का दायरा पारंपरिक पढ़ाई-लिखाई से बढ़कर डिजिटल कौशल को भी समेटने लगा है।
अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस का इतिहास
अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस की शुरुआत 1965 में ईरान के तेहरान में आयोजित विश्व शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में हुई। वहां उपस्थित प्रतिनिधियों ने शिक्षा और निरक्षरता के मुद्दे पर गंभीर चर्चा की।
इसके बाद 1966 में यूनेस्को (UNESCO) ने 8 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में घोषित किया। पहली बार यह दिवस 1967 में मनाया गया था। तब से यह दिन विश्व भर में पढ़ाई-लिखाई के महत्व को रेखांकित करता आ रहा है।
यह दिवस विश्व समुदाय को निरक्षरता के खिलाफ जागरूक करता है और साक्षरता को हर उम्र, भाषा, लिंग और क्षेत्र के लिए उतना ही अनिवार्य मानता है।
साक्षरता क्यों महत्वपूर्ण है?
साक्षरता के महत्व को कुछ प्रमुख बिंदुओं में समझा जा सकता है:
- मूलभूत मानव अधिकार: पढ़ना और लिखना हर व्यक्ति का अधिकार है जो उसकी गरिमा और समाज में सहभागिता सुनिश्चित करता है।
- स्वतंत्रता व आत्मनिर्भरता: साक्षर व्यक्ति न केवल खुद के लिए बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी बेहतर निर्णय ले सकता है।
- आर्थिक विकास में योगदान: पढ़ा-लिखा व्यक्ति रोजगार के बेहतर अवसर पा सकता है और देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बना सकता है।
- स्वास्थ्य व जीवन शैली में सुधार: स्वास्थ्य संबंधी जानकारी पढ़कर आत्मसुरक्षा और उचित उपचार सुनिश्चित करता है।
- सामाजिक समावेशन: साक्षरता समाज के सभी वर्गों को जोड़ती है और सामाजिक भेदभाव कम करती है।
- जीवन भर सीखने का माध्यम: साक्षरता से व्यक्ति नई-नई चीजें सीखते हुए समय के साथ विकसित होता रहता है।
विश्व स्तर पर कई करोड़ लोग अभी भी निरक्षर हैं, जिससे गरीबी, बीमारी और सामाजिक असमानता बनी रहती है।
साक्षरता के प्रभाव
सकारात्मक प्रभाव
- सशक्तिकरण: पढ़ा-लिखा व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होते हैं और अपना आत्मसम्मान बढ़ाते हैं।
- बेहतर रोजगार और आजीविका: साक्षरता रोजगार पाने और जीविका साधने के अवसर बढ़ाती है।
- सामाजिक भागीदारी में वृद्धि: साक्षर लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया, चुनावों और सामाजिक कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।
- स्वास्थ्य में सुधार: समझदारी से स्वास्थ्य संबंधी निर्णय ले पाते हैं।
- शिक्षा के चक्र को आगे बढ़ाना: माता-पिता के पढ़े-लिखे होने से बच्चों की शिक्षा में भी सुधार होता है।
नकारात्मक प्रभाव (निरक्षरता के दुष्परिणाम)
- सामाजिक बहिष्कार: निरक्षर लोग अक्सर समाज में अलग-थलग हो जाते हैं।
- ग़रीबी का चक्र: कम पढ़ा-लिखा होना रोजगार की कमी और गरीबी का कारण बनता है।
- स्वास्थ्य समस्याएं: असमझदारी से गलत निर्णय लेने से बीमारी बढ़ती है।
- डिजिटल युग में पिछड़ापन: डिजिटल कौशल की कमी सामाजिक और पेशेवर अवसरों को सीमित करती है।
अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 की थीम
साल 2025 की थीम है “डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना”।
आज का युग डिजिटल युग है, जहाँ कंप्यूटर, स्मार्टफोन और इंटरनेट के बिना जीवन के अनेकों पहलुओं में भाग लेना मुश्किल हो गया है। इसी संदर्भ में डिजिटल साक्षरता — यानी डिजिटल माध्यमों का सही, सुरक्षित और प्रभावी इस्तेमाल करना — बहुत जरूरी हो गया है।
यह थीम यह बताती है कि साक्षरता का महत्व केवल अक्षर ज्ञान तक सीमित नहीं रहा। इसके अलावा डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता, और मीडिया साक्षरता जैसे कौशल भी आवश्यक हो गए हैं।
अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस के उद्देश्य
अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:
- साक्षरता के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना: सरकारों, संस्थाओं और आम लोगों को जागरूक करना।
- समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना: सभी विशेष रूप से महिलाओं, वंचित वर्गों व कमजोर समूहों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करना।
- जीवन भर सीखने को प्रोत्साहित करना: लगातार कौशल वृद्धि और नयी शिक्षा की पहल।
- वैश्विक सहयोग को मजबूती देना: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निरक्षरता को समाप्त करने के लिए संयुक्त प्रयास।
- डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना: डिजिटल पदयात्रा में किसी को पीछे न छोड़ना।
- सशक्त व्यक्तियों का निर्माण: हर व्यक्ति को समाज और अर्थव्यवस्था में पूर्ण भागीदार बनाना।
भारत में साक्षरता वृद्धि के प्रयास
भारत में अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस का एक विशेष महत्व है। देश ने साक्षरता दर में कई सुधार किए हैं, फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में और पिछड़े वर्गों के बीच बड़ी चुनौती बाकी है।
सरकार ने ‘सर्व शिक्षा अभियान’, ‘डिजिटल इंडिया’, ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ जैसी योजनाओं के जरिए व्यापक स्तर पर शिक्षा और साक्षरता को बढ़ावा दिया है। 2020 की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी शिक्षा को और अधिक समावेशी, गुणवत्तापूर्ण और कौशल-आधारित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
साक्षरता दिवस कैसे मनाएं?
- स्कूलों में पढ़ने-लिखने के कार्यशालाएं और प्रतियोगिताएं।
- डिजिटल साक्षरता पर विशेष कार्यक्रम।
- पुस्तक दान और पुस्तकालयों का संचालन।
- सोशल मीडिया और जन जागरूकता अभियानों में भागीदारी।
- वयस्क शिक्षा केंद्रों का प्रोत्साहन।
- कहानी सुनाने, नाटक और कला गतिविधियों के आयोजन।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न 1: अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है?
उत्तर: यह हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है।
प्रश्न 2: अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब शुरू हुआ था?
उत्तर: इसे यूनेस्को ने 1966 में घोषित किया और पहली बार 1967 में मनाया गया।
प्रश्न 3: साक्षरता क्यों आवश्यक है?
उत्तर: साक्षरता मानव अधिकार है, यह व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक रूप से सशक्त बनाती है।
प्रश्न 4: 2025 की साक्षरता दिवस की थीम क्या है?
उत्तर: “डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना”।
प्रश्न 5: दुनिया में अभी भी कितने लोग निरक्षर हैं?
उत्तर: लगभग 739 मिलियन लोग अभी भी बुनियादी पढ़ने-लिखने में असमर्थ हैं।
प्रश्न 6: आप साक्षरता दिवस में कैसे भाग ले सकते हैं?
उत्तर: जागरूकता फैलाकर, पढ़ाने और सीखने के कार्यक्रमों में भाग लेकर आप योगदान दे सकते हैं।
निष्कर्ष
अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 हमें यह याद दिलाता है कि शिक्षा और साक्षरता हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और समाज की प्रगति की बुनियाद है। डिजिटल युग में साक्षरता का महत्व पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए हमें डिजिटल साक्षरता समेत विश्व स्तर पर सभी के लिए साक्षरता की सुविधा सुनिश्चित करनी होगी ताकि कोई पीछे न रह जाए।
सभी को मिलकर शिक्षा के इस उजाले को फैलाना चाहिए और एक समृद्ध, समान और शांतिपूर्ण विश्व की रचना करनी चाहिए।